संपर्क : 7454046894
इंटरनेट की जान कहाँ बसती है?
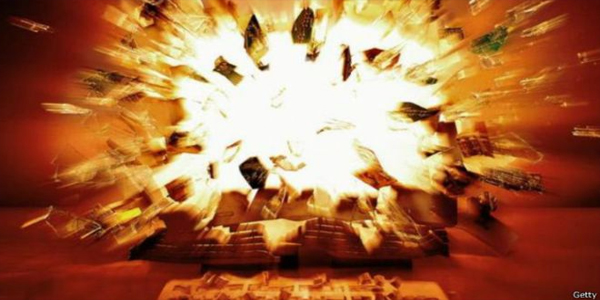
इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा. कम से कम हम लोग तो ऐसा ही सोचते हैं. तभी तो जब कोई चीज़ इंटरनेट पर काफ़ी ज्यादा वायरल हो जाती है चाहे वो किम कार्दाशियां की तस्वीरें हो या फिर द ड्रेस हैशटैग का वायरल होना हो, हम मजाक में कहते हैं कि ये 'ब्रेकिंग द इंटरनेट' जैसा है.
हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हमें ये मालूम है कि ऐसा होने वाला नहीं है. लेकिन क्या इंटरनेट को ब्रेक किया जा सकता है? अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, क्या हम इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं?
इस सवाल के जवाब का कुछ हिस्सा लंदन के डॉकलैंड ज़िले में मिलता है. कैनेरी वार्फ़ के उत्तर-पूर्व में एक बड़ी इमारत है, स्लेटी रंग वाली इस इमारत का बाहरी हिस्सा मेटल फ़ेंस से घिरा हुआ है. इस इमारत में कहीं कोई खिड़की नज़र नहीं आती है, लेकिन इमारत के बाहरी हिस्सों में सुरक्षा के लिए ढेरों कैमरे लगे हुए हैं.
30 इमारतों से चलता है इंटरनेट

लंदन की इमारत के बाहर किसी तरह का कोई होर्डिंग नहीं नजर आता है, जिससे ये पता नहीं चलता है कि यहां होता क्या है. लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया के लिए बेहद अहम इमारत है. दरअसल, ये लिंक्स की इमारत है. लिंक्स, यानी लंदन इंटरनेट एक्सचेंज.
दुनिया भर में होने वाले इंटरनेट ट्रैफ़िक एक्सचेंज के सबसे बड़े ठिकानों में एक है लिंक्स. लिंक्स जैसे बड़े एक्सचेंज दुनिया में और भी हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है. कटेंट डिलिवरी नेटवर्क क्लाउड फ़्लेयर के सीईओ मैथ्यू प्रिंस के मुताबिक लिंक्स जैसे एक्सचेंजों की संख्या 30 के आसपास होगी.
ऐसी इमारतें दुनिया भर में फैली हुई हैं, जहां एक से बढ़कर लोकप्रिय नेटवर्क प्रोवाइडरों के तार पहुंचते हैं. यानी, ऐसी इमारतों से ही इंटरनेट की दुनिया संचालित होती है. अगर इन इमारतों में कोई बाधा आ जाए, मसलन बिजली जाने से पावर कट हो या फिर भूकंप आ जाए तो इंटरनेट की दुनिया पर असर पड़ेगा.
मैथ्यू प्रिंस बताते हैं, "कभी कभी इंटरनेट की दुनिया कुछ हिस्सों में बाधित रहती है. ऐसे में अगर सभी 30 इमारतों को प्रभावित कर दिया जाए तो मोटे तौर पर इंटरनेट काम करना बंद कर देगा."
कितनी सुरक्षित है दुनिया?

हालांकि ऐसा होना इतना आसान भी नहीं है. टियर वन नेटवर्कों में लेवल 3 के चीफ़ टेक्निकल ऑफ़िसर जैक वाटर्स मानते हैं कि इन इमारतों के साथ साथ इंटरनेट की दुनिया भी काफ़ी सुरक्षित होती है.
उन्होंने बताया कि अब तक लेवल 3 की कई इमारतों में से किसी इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं हुई. हालांकि उन्होंने साफ़ किया कि हर इमारत की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और सुरक्षा के तमाम उपाय पहले से ही किए जाते रहे हैं.
ऐसे में, एक सवाल ये उठता है कि अगर इन इमारतों में लिंक को काट दिया जाए, तो इंटरनेट की दुनिया बाधित हो जाएगी? इस पर विचार करने से पहले हम देख लें कि दुनिया भर में असंख्य मील लंबी तारों के जरिए सूचनाएं एक्सचेंज हो रही हैं. इन तारों का बड़ा हिस्सा असुरक्षित है ख़ासकर जमीन के नीचे से गुज़रने वाले तार.
कई बार हादसों की वजह से भी इंटरनेट केबल प्रभावित होते हैं. कई बार भूकंप से या फिर पानी के अंदर जहाजों के एंकर से केबल प्रभावित होते हैं. माना जाता है कि 2008 में मिस्र सहित कुछ देशों में इंटरनेट इसी तरह की बाधा के चलते प्रभावित हुआ था.
समस्या की शुरुआत

लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अधारभूत ढांचों के साथ मुश्किलों का असर बहुत दूर तक नहीं पड़ता. ये पोलैंड में जन्मे अमरीकी इंजीनियर पॉल बारान के चलते संभव हो पाया था. 1960 के दशक में बारान उन चुनिंदा लोगों में थे जो ये सोचते थे कि संचार का तंत्र ऐसा होना चाहिए, जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं हो.
उन्होंने इस विषय पर कई अचरज भरे पर्चे लिखे, लेकिन तब उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता था. लेकिन वेल्स के कंप्यूटर साइंटिस्ट डोनल्ड डेविस की भी सोच बारान जैसी थी.
एक समय में दोनों एक ही दिशा में मौलिक ढंग से सोच रहे थे. डोनल्ड का आइडिया पैकेट स्विचिंग का था, जिसके तहत सूचनाओं को छोटे छोटे ब्लॉक या पैकेट में तोड़ने की बात शामिल थी. इन पैकटों को सबसे तेज़ उपलब्ध रुट के जरिए नेटवर्क में भेजने की कोशिश के तहत जोड़ दिया गया. अगर किसी रूट का सबसे अहम लिंक प्रभावित भी हो जाए तो संदेश दूसरे रास्ते के जरिए तय जगह तक पहुंचना चाहिए.

जैक वाटर्स के मुताबिक डोनल्ड डेविस की सोच काफ़ी महत्वपूर्ण और समय से कहीं आगे थी. वाटर्स कहते हैं, "इस विचार में संवाद के दोनों आखिरी सिरे महत्वपूर्ण थे, ना कि रूट, ये काफ़ी प्रभावशाली विचार था."
इसी सोच का नतीजा है कि केबल काटने या फिर डाटा सेंटर को ऑफ़ लाइन करने के बाद भी नेटवर्क को ज्यादा नुकसान नहीं होता है.
अगर सीरिया के पूरे इलाके को डिसकनेक्ट कर दिया जाए तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सीरियाई नेटवर्क के बीच आपसी संवाद खत्म हो जाएगा. ये ज़रूर होगा कि गूगल जैसी किसी बाहरी वेबसाइट को वहां देख पाना संभव नहीं होगा.
बढ़ रहे हैं हमले
हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि संचार के लिए इंटरनेट के रूट को अपने से तय करने की खूबी को इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें काफ़ी ज्यादा ट्रैफ़िक नेटवर्क पर डाल दिया जाता है जिसे डिनायल ऑफ़ सर्विसेज कहा जाता है, यानी इतना ज्यादा लोड जिसे सिस्टम संभाल ही नहीं पाए. ऐसे हमले अब खूब हो रहे हैं. इन ख़तरों को ध्यान में रखते हुए क्लाउड फ़्लेयर और दूसरे नेटवर्क सुरक्षा के इंतजाम करते हैं.

क्लाउड फ़्लेयर के सीईओ प्रिंस मानते हैं कि क्लाउड फ़्लेयर अपनी क्षमता से ज्यादा के नेटवर्क को बैड ट्रैफ़िक में बदल देता है ताकि सार्वजनिक वेबसाइट पर कोई खतरा नहीं हो. हालांकि इस समस्या के हल में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
प्रिंस बताते हैं, "निश्चित तौर पर हमले बढ़ रहे हैं. उन हमलों का आकार और स्केल दोनों बढ़ रहा है. ये इतना आसान हो गया है कि लोग कारोबारी प्रतिद्वंदिता में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं."

एक दूसरी बड़ी चिंता बीजीपी हाइजैकिंग को लेकर है. बीजीपी से मतलब है- बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. यह एक ही सिस्टम है जो इंटरनेट ट्रैफ़िक को बताता है कि सूचनाओं से भरे अरबों पैकेट को कहां जाना है.
लंबे समय से ये माना जा रहा था कि बीजीपी राउटर्स नेटवर्क में कई जगहों पर लगे होते हैं जो पैकेट को सही दिशा में भेजते रहते हैं. लेकिन हाल के सालों में ये पता चला है कि हैकर्स चाहें तो इन राउटर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं. इस हाईजैंकिंग के ज़रिए काफ़ी मात्राएं में सूचनाएं चुराई जा सकती हैं या फिर सूचनाओं पर नज़र रखी जा सकती है.
ओवरलोडेड ट्रैफ़िक का सच

इसके अलावा ये भी संभव है कि सूचनाओं के ट्रैफ़िक के बड़े हिस्से को ख़ुफ़िया ढंग से उन इलाकों में भेज दिया जाए जहां वे पहले से काफ़ी ज्यादा हैं. ऐसा कुछ सालों पहले तब हुआ जब पाकिस्तान की सरकार ने लोगों को यूट्यूब देखने से रोकने की कोशिश की.
पाकिस्तान में बीजीपी के रूट बदल दिए गए लेकिन ये सूचना दुनिया भर में पहुंच गई. तब बड़ी संख्या में लोग यूट्यूब नहीं देख पाए. नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोडेड हो गए. बीजीपी अपडेट्स के साथ राउटर्स की ओवरलोडिंग से इंटरनेट ऑफ़लाइन हो सकता है.
ट्रैफ़िक का रूट बदलने पर उन लोगों को काफ़ी मुश्किलें होती हैं जो सर्वर और ऑनलाइन सिस्टम को चालू रखने की कोशिश करते हैं. एक ब्लॉगर ने हाल में इस मसले पर लिखा है, "अपने लागिंग के दौरान जब मैंने आईपी एड्रेस देखने शुरू किए तो मुझे एक बात दिलचस्प लगी: सारे के सारे ट्रैफ़िक चीन से आ रहे थे."
इन सब कारणों से बाधा तो पैदा होती है लेकिन इंटरनेट के ब्रेक या ऑलाइन हो जाने जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होती. लेकिन इन सबसे इंटरनेट पूरी तरह ग़ायब हो चुका हो, ऐसा नहीं होता. मैसाच्यूट्स इंस्टीच्यूट ऑफ़ टेक्नालॉजी के प्रोफ़ेसर विंसेंट चान इस मसले पर कहते हैं, ऐसा अब तक नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इस पर सोचना भी नहीं चाहिए.
स्लो सिस्टम का राज

प्रोफ़ेसर कहते हैं, "मुझे लगता है कि पूरे इंटरनेट को रोकने का बड़ा हमला संभव है." चान मानते हैं कि आधारभूत ढांचे पर हमले से स्थायी नुकसान संभव नहीं हैं. वे बताते हैं कि एक हज़ार नोड वाले नेटवर्क में कोई एक नोड नष्ट हो जाए तो नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन अगर सभी हज़ार नोड प्रभावित हो जाएं तब मुश्किल हो सकती है.
चान ने कहा, "ऐसी सूरत में ये एक हज़ार नोड की नाकामी नहीं होगी बल्कि सिस्टम की नाकामी होगी." चान ये भी बताते हैं कि इंटरनेट में बाधा डालने के तरीके आ गए हैं जिसकी पहचान कर पाना खासा मुश्किल है. वे अपनी प्रयोगशाला में डाटा सिग्नल और उच्च स्तर के शोर को आपस में इंसर्ट करके प्रयोग कर रहे हैं.
इस प्रयोग के बारे में वे बताते हैं, "अगर आप किन्हीं सिग्नल के साथ पर्याप्त शोर को डालते हैं तब सिस्टम डाउन तो नहीं होगा लेकिन उसमें एरर का आना शुरू होगा और कई सारे पैकेटों को पढ़ पाना संभव नहीं होगा."

चान के मुताबिक इस समस्या से सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है, अपनी क्षमता का महज एक फीसदी तक काम कर पाता है. चान के मुताबिक कोई ना कोई इंटरनेट पर इस तरह से हमले कर सकता है. लेकिन तब इंटरनेट पूरी तरह ठप हो जाएगा, इसको लेकर चान को संदेह है. वे कहते हैं, "इंटरनेट पर हमले और उसकी सुरक्षा पर बातचीत होनी चाहिए. इस पर पहले पूरी तरह चर्चा नहीं हुई है."
कितनी बड़ी है मुश्किल?
हमारी आधुनिक दुनिया में बैंक, कारोबार, सरकारी व्यवस्थाएं, आपसी संवाद और उपकरण, इंटरनेट के ज़रिए ही चलते हैं. स्थानीय स्तर पर अस्थायी बाधाएं तो ठीक हैं लेकिन अगर वाकई इंटरनेट ठप हो, तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं.
इंटरनेट टैक्नालॉजी के नामचीन विशेषज्ञों में शामिल डैनी हिलिस ने टीईडी व्याख्यान में 2013 में कहा था कि असली मुश्किल ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि असली चुनौती कितनी बड़ी है.
हिलिस कहते हैं, "कोई इंटरनेट पर इस्तेमाल हो रही चीज़ों के बारे में पूरी तरह नहीं जानता. ऐसे में किसी प्रभावी हमले से इंटरनटे की दुनिया पर क्या असर होगा, हम नहीं जानते."

हालांकि हिलिस ये मानते हैं कि किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि इंटरनेट एक दिन क्रैश हो सकता है. वे कहते हैं, "जब प्लान ए ठीक से काम कर रहा हो तो किसी को प्लान बी की चिंता नहीं होती."
इंटरनेट की दुनिया लगातार बढ़ रही है. हमारी निर्भरता भी उस पर बढ़ रही है. ऐसे में उस पर खतरा भी बढ़ रहा है. लेकिन हममें से कोई उस ख़तरे के बारे में सोचना भी नहीं चाहता.
